अशोच्यान्नवशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।
गतासूनगातासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः
महाभारत के युध्द के समय अर्जुन अपने पूजनीय भीष्म पितामह और गुरू द्रोणाचार्य व धृतराष्ट पुत्रों को देखकर सोचते है कि – मै अपने जनों से युध्द कैसे करूंगा ऐसे भगवान श्री कृष्ण से कहते है। भगवान श्री कृष्ण करते हुए अर्जुन को समझाते हुए कहते है –
व्यख्या – श्री भगवान नें कहा – तुम न शोक करने के योग्य (मनुष्यों ) के लिए शोक करते हो और पण्डितों के समान वचनों को कहतें हो, परन्तु बुध्दिमान लोग मृतों के लिए अथवा जीवित प्राणियों के लिए शोक नहीं किया करते ।
श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं-
अर्थात् श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि – जो तुम भीष्म, द्रोणादि की हत्या के विषय में शोक कर रहे हो,
वे शोक करने योग्य नही हैं । भीष्म द्रोणादि की हत्या के विषय में प्रश्न है कि क्या वे वाच्यार्थ रूप से भरे है या लक्ष्यार्थ रूप से । यदि वाच्यार्थ रूप मानते हो तो वे महापुरूष हैं, महान् महिमावाले है, वे सदा अमर है, चिरंजीवी है। दूसरा पक्ष भी ठीक नही, क्योंकि शरीर नष्ट होनें वाली वस्तु है, सभी प्राणी सदैव मृत्यु ग्रस्त होते हैं। अतः मरणधर्मशील शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिये ।
प्रज्ञावादांश्च भाषसे – पण्डितों के जो विभिन्न मत है, उनका यह उदाहरण देते हो कि ‘कुल’ के क्षय होने से कुल धर्मनष्ट हो जाते है। मेरे पुत्रादि मर गये हैं- यह सोचकर मरे हुए का शोक नहीं करते परन्तु ये मेरे पुत्र मूर्ख, अभागे एवं दुराचारी उत्पन्न हुए है यह सोचकर बुध्दिमान, जीवितों के विषय में भी शोक नही करते
परन्तु विवेक पुरूष जीवित एवं मृत दोनों के विषय में नहीं सोचते । क्योंकि जीवन मृत्यु दोनों भाव अविद्या के कार्य है, वे स्वप्नमय पदार्थो के समान मिथ्या है। पण्डित लोग जीवन – मृ्त दोनों वस्तुओ को ब्रम्हा स्वरुप देखते हैं और शोक से परे हो जाते हैं।
गीता के उपदेश
टिप्पणी – अशोच्यान – शुच + यत प्रत्यय – न शोच्यः-
नञ तत्वपुरूष समास ।
अशोचः- शुच धातु मध्यम पुरूष एक वचन
प्रज्ञावादान – प्रज्ञानां वादाः – षष्ठी तत्वपुरूष
भाव से – भाष् से – भाष + मध्यम पुरूष एक वचन
गतासन – गताः असवः येषां ते, बहुब्रीहि समास
नानुशोचन्ति – अनु + शच् +लट् लकार प्रथम पुरूष बहुवचन
देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।
तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्थत्र न मुह्याति।।
जिस प्रकार जीवात्मा की इस देह में बाल्यावस्था, यौवन, वृध्दावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति भी होती है। इसलिए धीर पुरूष उस विषय में मोहित नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के कहनें का तात्पर्य है कि आत्मा सदैव एकरूप है, उसमें कभी विकार नहीं होता। तत्वतः आत्मा ही देहादि उपाधियों
से युक्त होता है और कौमार्य, यौवन वृध्दावस्था आदि अनेक अवस्थाओं को प्राप्त होता है। जीवात्मा ही पहले कुमारावस्था, पुनः यौवनवस्था, पुनः वृध्दास्था में प्रवेश करता है।
वह पहले स्थूल शरीरों को प्राप्त करता है। पुनः सूक्ष्म शरीरों में प्रवेश करता है। विनाश तो शरीरों का होता है, आत्मा का नहीं। ऐसा जानकार आत्मस्वरूप वेत्ता इस विषय में भ्रम नही करते ।
जिस तरह जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जीव सदैव सत्य एवं नित्य रहता है, उसी तरह आत्मा की सत्यता एवं नित्यता है विभिन्न जन्मों में आत्मा का सदभाव नित्य होता है।
यह जानकर आत्मस्वरूप को पहचानने वाले लोग आत्मा के विषय में यह निश्चित ज्ञान कर लेते हैं कि उत्पति विनाश देहादि का होता है, आत्मा का नहीं।
टिप्पणी – देहे = सप्तमी विभिक्ति एक वचन
देहिनः = देहिन् विभक्ति एक वचन
देहान्तरप्राप्ति = अन्यः देहः इति देहान्तरः
मयूव्यं सकादि तत्वपुरूष, तस्य प्राप्ति षष्ठि तत्वपुरूष
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टिन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः।।
प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की नित्यता तथा विषय संयोग की अनत्यता का निरूपण करते हुए इस प्रकार कहते हैं-
व्याख्या – असत पदार्थ (सुख- दुखादि ) की सत्ता नहीं होती है और सत् पदार्थ (आत्मा) का अभाव या ध्वंस नहीं होता। इस प्रकार इन दोनों (नित्य – अनित्य) का निर्णय तत्व वेत्ता पुरूषों द्वारा कर दिया गया है। किसी भी असत् पदार्थ की सत्ता नहीं होती है अर्थात जो सत पदार्थ नहीं है उनका सत्ता होना असम्भव है । और सत् पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने इन दोनों की सत्ता की यथार्थ रूप से जान लिया है। भगवान श्री कृष्ण के कथन की अभिप्राय यह है कि-
भीष्म पितामह आदि जनों के शरीर के विषय में यदि सोचों तो यह शरीर उनका न तो पूर्व में था और न आगे रहेगा अतः अनित्य है। इसका जो दर्शन हमें होता है औ जिससे हम यह समझ बैठते हैं कि शरीर की सत्ता है, भाव है यह विचार अयर्थाथ है। क्योंकि सत तो वही होगा जो शाश्वत होगा।
ऐसी दशा में शरीर से जो सम्बन्ध, संयोग होता है वह भी असत् विनाशशील है। अतः ऐसे असत् विषय को नित्य नहीं माना जा सकता है। अनित्य है उसका चिन्तन करना उसे शाश्वत मानना बहुत बड़ी भूल करना है।
टिप्पणी – असतः – न सत् इति असत् – षष्ठी विभक्ति एक वचन ।
इस श्लोक में सांख्य के सत्कार्यवाद और अद्वैत वेदान्त के असत्कार्यवाद दोनों ही एक साथ प्रतिपादन किया गया है। ‘असतः’ पद यहाँ परिवर्तनशील, शरीर, इन्द्रिय और उसकी सत्ता नहींं है इस कथन द्वारा भगवान ने यह भाव व्यक्त किया है कि शरीर आदि जिस काल में प्रतीत होते है, उसके पहले भी नहीं थे, वाद में भी नही रहेगे अतः वे जिस समय प्रतीत हो रहे है उस समय भी वस्तुतः नहीं है।
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिंद ततम् ।
विनाशामव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति।।
व्याख्य़ा – जिसके द्वारा यह सब संसार व्याप्त है, उसको ही नाश – रहित समझो। कोई भी इस अविनाशी का विनाश करने में समर्थ नहीं है।
अर्थात यह दृष्टिगोचर होनें वाला जगत् अविद्या से उत्पन्न है, असत है। यह जिस अत्यन्त सूक्ष्म, व्यापक, सद्रूप ब्रम्ह से व्याप्त है, उसे सत कहते है। यह सतरूप आत्मां विनाश का विषय नहीं बनता । अत्यन्त सूक्ष्म एवं अत्यन्त महान होने के कारण यह विनाश की क्रिया से व्याप्त नहीं हीता नित्य होता है। आत्मा परिपूर्ण है जैसे, आकाश शब्दरूप से सबको पूर्ण किये हैं।
टिप्पणी – इदं सर्व ततम् – शांकर वेदान्त का यह सिध्दान है कि यह सारा संसार जड़ं चेतन समूह ईश्वर से व्याप्त है। गीता और रामायण का भी यही भाव है कि ईश्वर अणु – अणु परमाणु -परमाणु में व्याप्त है। उपनिषद भी यही सिध्दान्त है –
य एवं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते।।
व्याख्या – जो व्यक्ति इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नही जानते, क्योकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है तथा न किसी के द्वारा मारा ही जाता है।अर्थात यह आत्मा आकाश की भाँति, कुटस्थ, नित्य है, असंग है, उदासीन है। अतः यह स्वयं किसी को न मारता है आकाश की भाँति विरवयव है। जैसे वृक्ष के चलनें पर उसमें आकाश चलता नहीं, वैसे आत्मा शान्त रहता है।
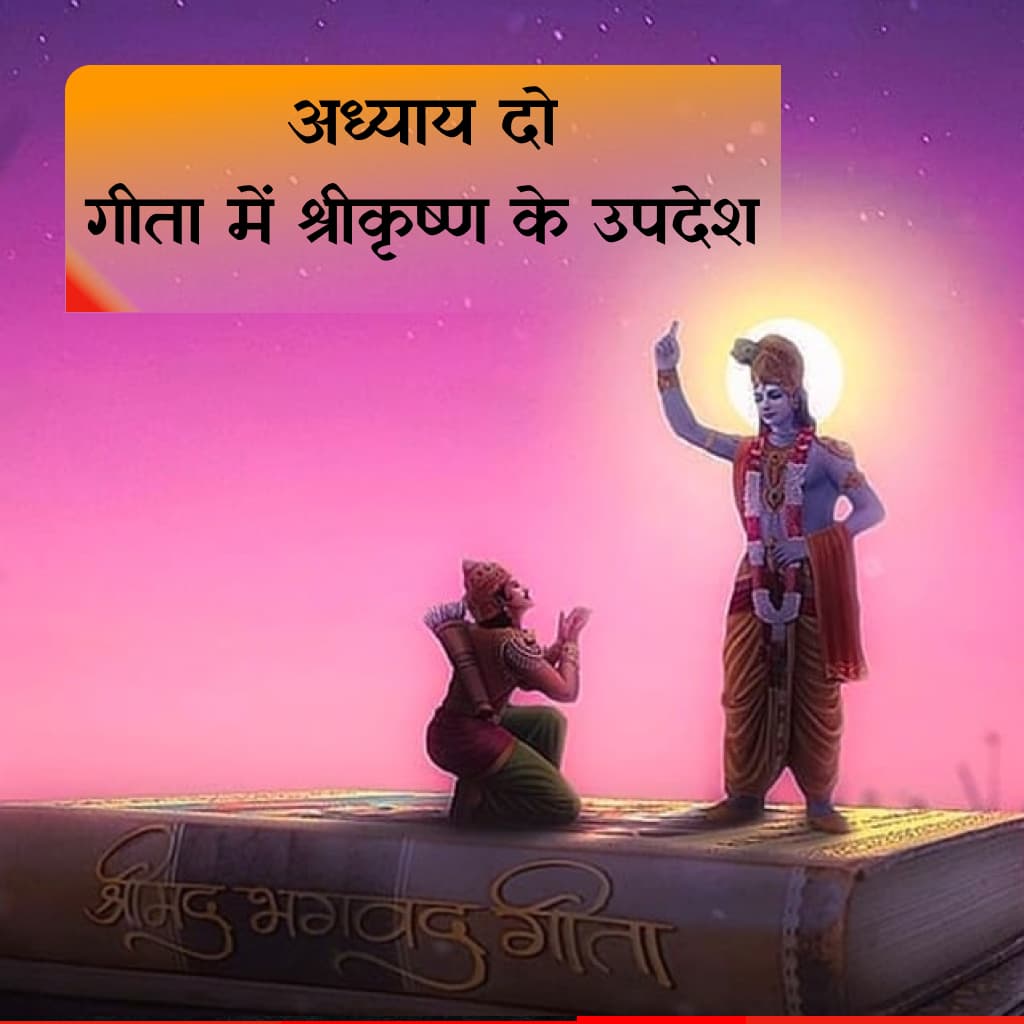
इस तरह जो अपने आपको कर्ता, भोक्ता, सुखी- दुखी मानते है वे आत्म तत्व को नही पहचानते ।
टिप्पणी – यहाँ लेखक आत्म और अनात्म में, सांख्य के पुरूष व प्रकृत में भेद कर रहा है।
एवं = एतद – द्वि एक वचन
वेत्ति = – प्रथम पुरूष एक वचन
हन्तारं = हन + तृच – द्वि0 एक वचन
हन्तारं हतम पीछे अर्जुन ने भगवान से कहा था ‘‘ मै इनको मारना नहीं चाहता औ वे यदि मुझे मार डालें तो मेरे लिए कल्याणकारी होगा।’’ बस इसी कथन के उत्तर में ही यह श्लोक को मारता नहीं है और न वह किसी के द्वारा मारा जाता है। मरना तो शरीर का धर्म है और मारना भी उसी का कार्य ।
न जायते म्रियते वा कदाचि-
त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
न हन्यते हन्यमाने शरीर ।।
व्याख्या – यह आत्मा न कभी उत्पन्न होता है अथवा न कभी मरता है और उत्पन्न होकर न पुनः होने वाला है । यह अजन्मा, नित्य , सनातन अनादि है। शरीर के मारे जानें पर भी यह नहीं मरता ।
अर्थात् भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा इस कारण न तो मारी जाती है और न मरती है और न मरती है क्योंकि इसमें उत्पति तथा विनाश ही नहीं है अर्थात न तो इसका जन्म होता है और न इसकी मृत्यु होती है। न इसका आदि है और न अन्त है। न नित्य है, शाश्वतं है, पुरातन है, अतः शरीर के मारे जानें पर यह नहीं मरती है।
टिप्पणी – न जायते म्रियते – उत्पत्ति, अस्तित्व, वृध्दि विपरिणाम (रूपान्तर को प्राप्त होना) अपक्षय, विनाश ये छः विकार शरीर के बतलाये हैं। इस श्लोक में अजः आदि पदों द्वारा आत्मा में इन विकारों का अभाव बतलाया गया है।
जायते = जन् कर्मवाच्य प्रथम पुरूष एक वचन
म्रियते = मृ कर्मवाच्य
हन्माने = हन + कर्मवाच्य + शानच् प्रत्यय सप्तमी एक वचन
हन्यते = हन् कर्मवाच्य प्रथम पुरूष एक वचन ।
कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः
पृच्छापि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं बूहि तन्में
शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।।
प्रसंग – अर्जुन भगवान श्रीमद्भगद्गीता में कहते कि मै अल्पज्ञ होने के कारण भ्रण में पड़ा हुआ हूँ । अतः आप मुझे कल्याणकारी मार्ग बताये।
व्याख्या – कायरता या अविद्या के दोष के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और मेरा चित्त धर्म के विषय में भ्रम में पड़ा हुआ है, अतएवं मै आपसे पूछता हूं कि जो निश्चित रूप से कल्याण का मार्ग हो उसे मुझे बताइये । मै आपका शिष्य हूँ मुझे उपदेश दीजिए।
वासांसि जीर्णानियथा विहाय
नवानि गृहणाति नरोपरण।
न्यन्यानि संयाति नवानि देही।।
प्रसंग – भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अविनाशी आत्मा और नश्वर शरीर के स्वरूप को समझाते हुए कहते है-
व्याख्या – जिस प्रकार मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्यागकर दूसरे नये वस्त्रों को धारण करता है उसी प्रकार जीवात्मा भी जीर्ण शरीरों को छोड़कर दूसरे नये शरीरों को प्राप्त करता है।
अर्थात् जिस प्रकार सूर्य पूर्व एवं पश्चिम के पर्वत का आश्रय लेकर उदित – अस्त होता है, फिर भी उसके स्वरूप में कुछ अन्तर नहीं आता। वैसे ही शरीर जन्म या शरीर त्याग से आत्मा औषधिक रूप से विकारी होता है। जैसे पुराने वस्त्रों के उतारने और नये को पहनने से शरीर के नाम रूप में अन्तर होता है, परन्तु आत्मा में नहीं वैसे ही शरीरों की मृत्य, एवं जन्म में नामरूपात्मक वैचित्रय होता है आत्मा का नहीं। आत्मा निरवयव है, शरीरादि से भिन्न एवं अविकारी है, नित्य है, ऐसा आत्म स्वरूप सिध्द होता है